‘उमराव जान’ से बेहतर कोई हमराही हो ही नहीं सकता





उमराव जान : पर ख़त्म हुआ क्या अभी भी जंग का सफ़र प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक अज्ञेय की ये पंक्तियां जेहन में अपने आप आ जाती हैं जब मैं प्रभात पाण्डेय सर को पढ़ती हूँ-
“यो मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ
काव्य-तत्त्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ?
चाहता हूँ आप मुझे एक-एक शब्द पर सराहते हुए पढ़ें।
पर प्रतिमा- अरे, वह तो
जैसी आप को रुचे आप स्वयं गढ़ें।’’ ये शब्द पाण्डेय सर के लिए सटीक इसलिए बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम और अनुसन्धान से अपनी कृति ‘उमराव जान’ को रचा है। अज्ञेय की ये पंक्तियाँ घटित हुई, जब मैंने वरिष्ठ साहित्यकार प्रभात पाण्डेय सर की कृति ‘उमराव जान’ पढ़ी। इन दिनों जितने समय तक ‘उमराव जान’ के साथ मेरा सफ़र चला, लगा जैसे ‘उमराव जान’ से बेहतर कोई हमराही हो ही नहीं सकता। एक-एक शब्दों पर मैंने कवि के काव्य-सौष्ठव को सराहा। चूँकि प्रतिमान गढ़ने का हक़ मिल ही गया था तो मैंने देखा कि इस कृति के सारे प्रतिमान ध्वस्त होती पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्रीवादी विमर्श की एक चीख है।
इस पूरे सफ़र में कभी-कभी मुझे लगा कि पाण्डेय जी मुद्दे से भटक रहे हैं, वो आधुनिक उमराव से अचानक पुरातन सीता, अहिल्या अदि की बातें क्यों करने लगे? फिर मैं जब रचना में डूबे हुए आगे बढती हूँ और अगली डुबकी पर मुझे नारी-विमर्श के दिग्दर्शन होते हैं तब मुझे कोई आश्चयर्य नहीं रह जाता कि बात बस उमराव ,सीता, अहिल्या या मुझ जैसी किसी एक स्त्री की नहीं वरन बात उस पुरे स्त्री समाज की है जो सदियों से पीड़ित और शोषित होती आई है।
जैसा की हम सब जानते हैं कि उमराव जान अवध रियासत की एक मशहूर तवायफ थी। ‘उसी के जीवट संघर्ष को ज्वलंतता से उजागर करती कृति है ‘उमराव जान’। मिर्जा मोहम्मद रुसवा हादी के उपन्यास के अतिरिक्त उमराव के बारे में अधिक रचनाएँ नहीं है जिससे उसका ठीक-ठीक चरित्रांकन किया जा सके। जैसा कि सभी को ज्ञात है आदरणीय पाण्डेय जी ने अपने जीवन का एक कालखण्ड नबाबों की इस नगरी लखनऊ में गुजारा है और संभवतया यही कारण है कि वे इस कृति के साथ न्याय कर पाएँ हैं।
जब हम कविता के साथ-साथ यात्रा पर निकलते हैं तब उस रियासत-कालीन समाज के आसानी से दर्शन हो जाते हैं। जहाँ तक भाषा का सवाल है वह ‘आम-फहम हिन्दुस्तानी’ वाली जबान जिसे लोग कहा करते थे, वही है। अरबी-फारसी के साथ ही कहीं-कहीं सुन्दर हिंदी शब्दों के छोटे-छोटे वाक्यांश मन को मोह लेते हैं।
यथा-
सर्राफ़े पर हीरे-जवाहिरात
पोर-नगीने जड़ें ज़ेवरात
इफ़रात सोने के सिक्के चमचमाते
चमचमाते मोती- चमचमाते अल्मास
चमचमाते नीलम-पन्ना-पुखराज।
बज्जाज की दुकान पर
बेशुमार हलचल
मचल-मचल ढाका की मलमल
पसर-पसर जाती लखनवी चिकन पर।
सामान्य से हिन्दी शब्दों का अमूल्य प्रयोग
हारे को सहयोग
कहाँ ऐसा भाग्य
कहाँ ऐसा संयोग
अरबी-फारसी के साथ ही तद्भव शब्दावली का सुन्दर प्रयोग ऊपर की कुछ पंक्तियों में हम देख चुके हैं। इन पंक्तियों में विविधता लाते हुए कवि ने तत्सम शब्दावली का सुन्दर प्रयोग किया है , जो बड़ा ही श्लाघनीय बन पड़ा है।
अनहद नाद
अजीबो ग़रीब उन्माद
जैसे कोटि-कोटि शंख
जैसे तितली के पंख
क़तरा- क़तरा फड़फड़ाता
जब उसका दुपट्टा हवा में लहराता।
कवि के ज्ञान का फलक बहुत विस्तृत रहा है। नाथ-पंथी हठ-योग साधना में ‘अनहद-नाद’ का अपना एक विशिष्ट महत्व है। कहा जाता है की जैसे-जैसे साधक की कुण्डलिनी षट्चक्रों का भेदन करती है; वैसे-वैसे साधक को परमात्मा से सामिप्य का बोध होता है। इस सामिप्य की प्रक्रिया में उसे एक आध्यात्मिक संगीत सुनने को मिलता है जिसे ‘अनहद नाद’ कहते हैं।
कबीर ने कहा भी है-
"उलटे पवन चक्र बेधा, मेरुदंड सरपूरा।
गगन गरजि मन सुन्नि समाना, बाजे अनहद तूरा।।’’
ऐसे शब्दों के समायोजन से कविता दुरूह नहीं अपितु रोचक के साथ ही सामान्य से विशिष्ट के लिए भी प्रिय हो जाती है।
तत्सम शब्दावली एक और सुन्दर उदहारण-
कंठ में सिंहल के मोतियों की माला
नाजुक कमर को करधनी ने सम्हाला
सुडौल गुल्फ पर
सोने की पैजनियों की चमक
वेणी के फूल- उनकी महक।
स्त्री मनोविज्ञान के पारखी कवि को जब हम कहते हुए सुनते हैं-
बात तुम्हारी सही-सही ही
औरत को रश्क औरत से ही
होता है वह जब-जब जहां
होता है वह बस बेइंतिहा।
पर इस बेइंतिहा से किसी को सरोकार नहीं, रश्क करना तो जैसे जन्मजात सीख के आते है और ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। इस पूरी कृति में कवि का कभी-कभी उमराव जान से साक्षात्कार होता है, कभी उमराव जान प्रतिउत्तर देती है तो कभी चुपचाप सी हो जाती है..कभी-कभी घंटों एकालाप भी चलता रहता है परन्तु इससे कथा-सूत्र में कहीं बिखराव नहीं आता।
तुम्हें हुआ क्या
गुफ़्तगू का सिलसिला रुक क्यों गया
अभी-अभी बतियाती
अभी गुमसुम
बैठे ही बैठे कहां खो गई तुम।
एक के बाद एक कथा जुडती जाती है कभी आदिकालीन सीता, अहिल्या और द्रौपदी आदि की आवाज कवि बुलंद करता है तो कभी रियासतकालीन बेगमों की व्यथा से हमें रूबरू कराता है। वो रंगीनियों में दबी हुई चीख को भी तलाश कर लेता है। एक औरत से दूसरी औरत हरेक की पीड़ा सुनता हुआ कवि भला कुदसिया महल की पीड़ा से बेखबर कैसे रहता? रंगमहल की रंगीनियों में दबी बेगम कुदसिया महल की पीड़ा की कहानी मन को झकझोर देती है।
पहला शौहर मीर हैदर
फिर जो होना था नहीं
वही हो गया
नीबू के शर्बत में मिलाकर संखिया
कुदसिया महल ने ख़ुद ही पी लिया।
शहर तमाम स्याह कपड़े पहन के
शामिल जनाजे में कुदासिया महल के
मातम ही मातम अवध तमाम
मुहर्रम-से माहौल में डूबा अवाम।
शहर तमाम स्याह कपड़े पहन के ..में अलंकार का उचित निर्वाह कवि ने किया है और इसके लिए किसी विशेष प्रयोजन की आवश्यकता भी नहीं पड़ी।
वार्तालाप जारी है...
तुमने देखा तो उमराव जान
जिन्हें जूतियों बिन न चलने की आदत
तमाम रात नंगे पांव चलती रहीं
देखा था चेहरा तक न जिनका किसी ने
बेनक़ाब दरबदर वे भटकती रहीं।
लखनऊ के गुंबदों के अलग ही नज़ारे
फिरंगियों को मगर यह तनिक न भाया
कितने ही मकानों को उन्होंने गिराया
मंदिर गिरे
मस्जिदें गिरीं
उन जालिमों के लिए क्या मंदिर या क्या मस्जिद ...वे कौन सा यहाँ पूजा या इबादत करने आय थे?
हजरत महल की अगुआई में
सबने शपथ यह लिया-
कि हाथों में कुरान और तुलसी-गंगाजल
कि हिन्दुस्तान से फिरंगी जब तक जाते न निकल
बांधे सर पर क़फ़न
थामे हाथ में तलवार
अवध का बच्चा-बच्चा रहेगा तैयार।
‘हाथों में कुरान और तुलसी-गंगाजल’ ...के द्वारा वे ‘गंगा-जमुनी तहजीब’ की बात करते हुए एक समतामूलक मार्ग प्रसस्त करते हैं, जिसकी आज महती आवश्यकता है।
इधर के बांकुड़े मगर तनिक न डोले
ग़ज़ब का जुनून
ग़ज़ब की लड़ाई
गोरों के हाथ एक इंच जमीन न आई।
बेगम हजरत महल और उनकी सेना की शौर्य गाथा को उचित स्थान देते हुए तारीखों का पूरा व्योरा यहाँ दिया गया है।
पच्चीस फरवरी-सुबह के बजे होंगे चार
हजरत महल ख़ुद हो हाथी पर सवार
साथ-साथ उनके बिरजीश कदर
हाज़िर थीं वे आलमबाग़ मोर्चे पर।
एक बार फिर से सब बेगम हजरत महल की अगुआई में कसम खाते हैं.....
लगा मिट्टी का तिलक
सबने क़सम ये खाई-
मुठभेड़ इस बार की इस पार या उस पार....
कर्मवाद में भरोसा रखने के बाद भी जब भाग्य साथ नहीं देता तब कमोबेश यही विचार आते हैं-
मद्धिम कब होती है तक़दीर की लिखाई
लकीरें हाथ की ही फिर आड़े हाथ आईं
कैसे सब हाथ आ के भी छीन जाता हैं...क्यों होनी को हम टाल नहीं सकते... उस पर हमारा वश नहीं चलता..
सच-सच बतलाना उमराव जान
साथ तुम्हारें यह क्यों हुआ
कि ग़दर पर ग़दर
कि क़हरे वाकियात एक-एक कर
होते रहे पेशेनज़र....
सच तो ये है उमराव जान
सदरुन्निसा से नवाब बेगम
उमत-उल-ज़ोहरा से बहू बेगम
कि परियां
कि बेगमें
किस-किस की हम बातें करें
कि महक परी से इफ्तखारुन्निसा
कि इफ्तखारुन्निसा से हजरत महल
इस क़दर जनानखाना की चहल-पहल
कि अमीरन
कि उमराव
कि उमराव जान
मुक़ाम दर मुक़ाम
औरत ही खोती अपनी पहचान।
यही सच है जब वह पिता के घर होती है, पिता से ही उसकी पहचान होती है और पत्नी बनते ही एक नया नाम जुड़ जाता है। सच तो ये है कि उसकी अपनी कोई पहचान होती ही नहीं..इस पितृ सतात्मक समाज ने उसे अपने वजूद से जुड़ने ही नहीं दिया। दी गई एक ऐसी पहचान जिससे पुरुषत्व का महत्त्व बरकरार रहे।
सच तो यह उमराव जान
तुम महज़ परी नहीं
माशूक़ा-ए-ख़ास भी तुम किसी की नहीं
माँ-बहन-बेटी और बनके जाया
चौखट-चौखट रिश्ता तुमने ही निभाया
तिस पर भी इन मर्दों का हाल
टस से मस तनिक न हुआ इनका ख़याल
नज़र-नज़र तो इनके महज़ हुस्नोजमाल।
बेवजह चाहत कि इनका आगोश
अरे, बघनखे सब
सब एहसान फ़रामोश।
ये महज उमराव जान नहीं हरेक स्त्री का दर्द है। बचपन से यौवन , प्रौढ़ होने से बुढ़ापे तक हरेक रिश्ते में खुद को मिटा के भी निभा देने वाली भले खुद को खपा दे पर उस योगदान को बहुत कमतर आंका जाता रहा है और यह सदियों से हो रहा..आज भी जारी है।
देखा उमराव जान
तुमने देखा तो
अनारकलियों पर गुज़रता जो-जो
ज़िल्ले इलाही उन्हें जीने नहीं देता
और सलीम तो सलीम
उन्हें मरने नहीं देता।
रूपमती को बाज बहादुर से प्यार
बेवजह मुग़लिया को यह न स्वीकार।
अशोक वाटिकाएं
उन में अब भी सीताएं
भयभीत-आतंकित उतनी ही नजर आएं।
अंधे धृतराष्ट्रों के अंधे दरबार
द्रौपदियों का चीर-हरण अब भी द्वार-द्वार।
दहलीज़ दर दहलीज़ घटाएं घनघोर
अहल्या ही अहल्या नज़र आती चारों ओर
महज़ कहने को है ख़त्म देवदासियों की प्रथा
पर घर-घर की ड्योढ़ी यों की अब भी वही कथा।
कवि वाल्मीकि की सीता, अहिल्या से लेके वेदव्यास की द्रौपदी आदि पात्रों तक ही सीमित नहीं रहता..वह वर्षों से हो रहे इस शोषण के स्वर का साक्षी भी है। वह अपनी धुन में कहता जाता है जिसके कान से खून निकलने लगे या यदि किसी का पुरुषत्व इस बात को सुनके आहत हो तो उसकी मर्जी; क्योंकि कवि तो चाहता है कि आप उसे सराहते हुए पढ़ें...बाकि प्रतिमान जैसा आपका मन करें गढ़ें।
जब मैं पढ़ती हूँ-
धर्म और मज़हब की बात
ये उनकी बात है
पर जीने का हक़ औरत का
नहीं खैरात है।
मन करता है कि पूछूं कि कवि! इतने तल्ख़ लहजे में इतनी कड़वी पर सच्ची बात कैसे लिख जाते हो? क्या किसी को बुरा नहीं लगता जब ‘आदमियत’ पर सवाल उठाते-उठाते बात महज ‘आदमी’ तक आ के रुक जाती है? क्या किसी के अहं को ठेस लगाए बिना ये लिख लेते हो? सच-सच बताना क्या खुद को भी नाराज नहीं किया जब ‘स्त्री’.. ‘स्त्री’.. ‘स्त्री’.. की आवाज उठाते हो ...सिर्फ स्त्री की ही सुनते हो? क्या मन नहीं कहता की बंद करो यूँ ‘औरत’ की पुरजोर आवाज बुलंद करना...बंद करो ये पुरजोर आजमाइश... क्यों सीता की मूक आवाज किसी और को नहीं सुनाई देती? क्यों अंधों और बहरों के भीड़ में खड़ी सैरेन्ध्री की पुकार सुन के तुम चीत्कार उठते हो? क्यों मुझ जैसे जाने कितनी स्त्रियों का दर्द इस पुरुष समाज में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देता है।( ये विचार मुझे उमराव जान के साथ सफ़र पर जाते हुए आए )
सच तो है उमराव जान
कि अब जा के
तुमने पाया है
सच्चा कद्रदान
प्रभात पाण्डेय सर आपकी इस रचना ने मुझमें माधुर्य और औदात्य कम ओज का संचार अधिक कर दिया है। बहुत सारे विज्ञ मंडली और अध्येता वर्ग ने अपने-अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया आपको प्रेषित की होगी...हो सकता कोई मेरी इस मत से सहमत हो, न भी हो, परन्तु मेरे जो मनोभाव हैं वो तब भी वहीँ रहेंगे। मैं नहीं सोच पा रही कि इसे ‘महाकाव्य’ कहूँ या ‘लम्बी कविता’। जो भी हो आधुनिक हिन्दी साहित्य को आपने यह अमूल्य निधि समर्पित की, आपकी साहित्य-साधना को जन-जन उमराव जान के साथ सफ़र पर निकल कर देख सकता है। कितनी मेहनत और लगन से यह कृति रचित है इसकी एक-एक पंक्ति को पढ़ कर समझा जा सकता है। आपका लेखन कर्म आगे भी अनवरत क्रियाशील रहे...मेरे माटी की महक मुझतक लाल सलाम भेजती रहे..
आदर और विनय के साथ
आपकी ही कुलांश
डॉ. रिंकी रविकांत

Related Posts
Post Comments


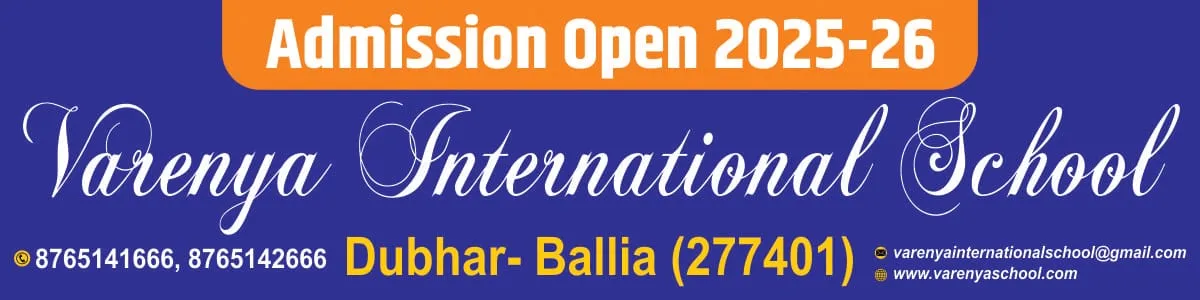










Comments